भारतीय संस्कृति
भारतीय संस्कृति
भारत के बहु-सांस्कृतिक भण्डार और विश्वविख्यात विरासत के सतत अनुस्मारक के रूप मेंभारतीय इतिहास के तीन हज़ार से अधिक वर्ष की जानकारी और अनेक सभ्यताओं के विषय में बताया गया है। भारत के निवासी और उनकी जीवन शैलियाँ, उनके नृत्य और संगीत शैलियाँ,कला और हस्तकला जैसे अन्य अनेक तत्त्व भारतीय संस्कृति और विरासत के विभिन्न वर्ण प्रस्तुत किए गए हैं, जो देश की राष्ट्रीयता का सच्चा चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस खण्ड में उन सभी तत्वों को शामिल किया गया है जो भारत की संस्कृति और विरासत के प्रतीक हैं।
800 ई. से 1200 ई. का काल आर्थिक और सामाजिक जीवन तथा धर्म के लिए उपयुक्त है। आर्थिक व्यवस्था, समाज, धार्मिक विश्वास तथा मानव विचार राजनीति से कहीं कम परिवर्तनशील है। इसीलिए ऐसी कई विशेषताएँ जो नौवीं शताब्दी के पूर्व पायी जाती थीं, अभी भी ज़ारी थीं। पर साथ ही कुछ ऐसी भी बातें थीं, जिससे इस काल को पहले के युग से भिन्न माना जाता है। सामान्यतः इस ऐतिहासिक काल में नए तत्वों के साथ पुराने तत्त्व भी विद्यमान रहते हैं, पर परिवर्तन की दिशाएँ भिन्न रहती हैं।
उत्तर काल में यह काल सामान्यतः जड़ता तथा ह्रास का काल माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह था कि सातवीं शताब्दी और दसवीं शताब्दी के बीच वाणिज्य और व्यापार में गतिरोध आ गया था। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में नगरों तथा नागरिक जीवन का ह्रास हुआ। वाणिज्य और व्यापार में गतिरोध का मुख्य कारण पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन था। जिसके साथ भारत का बड़े पैमाने पर तथा मुनाफ़े का व्यापार होता था। भारत में कभी भी बड़ी मात्रा में सोने और चाँदी के खनन का काम नहीं हुआ। सोना और चाँदी जिसके लिए भारत विख्यात था, वह भारत के लाभकारी व्यापार के कारण था क्योंकि मुनाफ़े के रूप में यहाँ सोना और चाँदी आते थे। इस्लाम के उदय से भी, जिससे सासानीद (ईरानी) जैसे प्राचीन साम्राज्यों का पतन हो गया, भारत के व्यापार और विशेष कर ज़मीन के रास्ते होने वाले व्यापार पर बहुत असर पड़ा। परिणामस्वरूप उत्तरी भारत में आठवीं और दसवीं शताब्दी के बीच नई स्वर्ण मुद्राओं की बहुत कमी हो गई। पश्चिम एशियातथा उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत और शक्तिशाली अरब साम्राज्य में ऐसे कई क्षेत्र शामिल थे जिनमें बड़ी मात्रा में ख़ानों से स्वर्ण निकाला जाता था। अरब स्वयं भी समुद्र प्रेमी व्यक्ति थे। भारतीय कपड़ों, मसालों तथा लोबान के लिए अमीर अरब शासकों की माँग के कारण भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीपों को मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता था। नौवीं और दसवीं शताब्दी के बीच कई अरब यात्री पश्चिमी तट के नगरों में आए और उन्होंने देश की तत्कालीन स्थिति का विवरण किया है। दसवीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में विदेश व्यापार और वाणिज्य में धीरे-धीरे फिर वृद्धि हुई। व्यापार के इस पुनरुत्थान से सबसे अधिक लाभ मालवाऔर गुजरात को पहुँचा। गुजरात में चंपानेर और अंकिलेश्वर जैसे कई नगरों की नींव इसी काल में पड़ी। उन दिनों भारत की जनसंख्या दस करोड़ से भी कम थी, अर्थात आज की तुलना में, छटे हिस्से से भी कम थी। देश का एक बड़ा भाग जंगलों से ढका था जिनमें जंगली पशुओं के अलावा ऐसे क़बीले थे जो राहगीरों को लूट लेते थे। नदियों पर पुल नहीं थे और बरसात के मौसम में सड़कें बहुत ख़राब हो जाती थीं। इन कारणो से उन दिनों यात्रा, चाहे व्यापार हो या फिर शौक़ के लिए, कभी भी खतरे से ख़ाली नहीं थी। सुरक्षा के ध्यान से व्यापारी तथा अन्य लोग कारवों में चलते थे जिसकी सुरक्षा उनके अपने सैनिक करते थे। इसके बावजूद कभी-कभी साहसी लुटेरे उन्हें लूट लेते थे।
भारत और चीन का व्यापार
भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार स्वयं में महत्त्वपूर्ण तो था ही इसके साथ-साथ वह भारत और चीन के व्यापार के लिए केन्द्र का कार्य भी करता था। आमतौर पर चीनी जहाज़ मोलस्का द्वीपों के आगे नहीं आते थे। उधर भारत और चीन के बीच का सड़क मार्ग उस काल में तुर्क, अरब तथा चीनियों के बीच संघर्ष के कारण सुरक्षित नहीं रह गया था। इसके स्थान पर भारत और चीन के बीच का समुद्री मार्ग अधिक महत्त्व का होता जा रहा था। चीन के विदेश व्यापार के लिए वहाँ का प्रमुख बंदरगाह कैटन, या जैसा कि अरब यात्री पुकारते थे, क़ाफु था। भारत से बौद्ध विद्वान भी समुद्र मार्ग से चीन जाते थे। चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि दसवीं शताब्दी के अंत तथा ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में चीनी राजदरबार में जितने भारतीय भिक्षु थे, उतने चीन के इतिहास में पहले कभी नहीं रहे। कुछ और पहले के काल के चीनी वृत्तान्त के अनुसार कैटन नदी भारत, फ़ारस और अरब से आने वाले जहाजों से भरी रहती थी। इसके अलवा कैटन में तीन हिन्दू मन्दिर थे जिनमें भारतीय ब्राह्मण रहते थे। चीनी समुद्र में भारतीयों की उपस्थिति के बारे में हमें जापानी सूत्रों से भी पता चलता है। इनके अनुसार जापान में कपास के परिचय का श्रेय दो भारतीयों को है। जो अपनी समुद्री यात्रा के दौरान लहरों के ज़ोर से ग़लती से जापान पहुँच गए थे। भारतीय शासकों, विशेषकर बंगाल के पाल, सेनतथा दक्षिण के पल्लव और चोल वंश के शासकों ने चीनी सम्राटों के दरबारों में अपने राजदूत भेज कर इस व्यापार को और उत्साहित करने की चेष्टा की। चीन के साथ भारत के व्यापार में बाधा डालने वाले मलाया तथा अन्य पड़ोसी देशों के विरुद्ध चोल शासक राजेन्द्र प्रथम ने अपनी नौसेना भेजी। चीन के साथ व्यापार करने वाले देशों को इतना लाभ होता था कि तेरहवीं शताब्दी में चीनी सरकार ने वहाँ से सोने और चाँदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की चेष्टा की। धीरे-धीरे भारत का व्यापार अरबों और चीनियों के मुक़ाबले कम होता गया क्योंकि इन व्यापारियों के जहाज़ भारतीय जहाजों से बड़े और अधिक तेज़ थे। कहा जाता है कि चीनी जहाज़ कई मंज़िल होते थे और उनमें चार सौ सैनिकों के अलावा छः सौ यात्री चल सकते थें चीनी जहाजों के विकास में कुतुबनुमा की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। यह आविष्कार चीन से दसवीं शताब्दी में पश्चिम पहुँचा। अब तक भारतीय विज्ञान तथा तकनीक पीछे पड़ते जा रहे थे।
पश्चिम के साथ भारत का व्यापार दसवीं शताब्दी के बाद ही तेज़ हो सका, पर दक्षिण-पूर्व एशिया तथा चीन के साथ उसका व्यापार बारहवीं शताब्दी तक धीरे-धीरे बढ़ता ही गया। इस व्यापार में भारत तथा बंगाल की मुख्य भूमिका थी। इन क्षेत्रों की सम्पत्ति और समृद्धी का भी यही प्रमुख कारण था।
सामंतवादी व्यवस्था
परिणामस्वरूप इस काल के राज्यों में कई ऐसे क्षेत्र शामिल थे जिन पर पराजित अथवा अधीन राजाओं का प्रभुत्व था और वे अपनी स्वाधीनता की घोषणा करने की ताक में लगे रहते थे। इसके अलावा राज्यों के कई क्षेत्रों में ऐसे अधिकारी थे, जो अधीन भूमि को पुश्तैनी जायदाद मानते थे। कालान्तर में इन अधिकारियों का पद भी वंशागत हो गया। बंगाल के एक परिवार से चार पुश्तों के सदस्य महामंत्री थे। इसी प्रकार सरकार के कई पद कुछ ही अधिकारियों के लिए सुरक्षित हो गए। इन वंशागत अधिकारियों ने धीरे-धीरे प्रशासने के कई कार्य अपने हाथों में ले लिए। यह न केवल लगान निर्धारित तथा वसूल करने का कार्य करते थे, बल्कि इन्होंने अधिक से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने हाथों में लिया और ये न्यायाधीश भी बन बैठे और अपने ही बल पर ऐसे मामलों में ज़ुर्माना तक करने लगे, जो पहले राजा की ओर से विशेषाधिकार के रूप में दिए गए थे। ये अपने क्षेत्र में पाए गए ख़ज़ानों पर भी अपने अधिकार का दावा करते थे, जबकि क़ायदे से इन पर राजा का अधिकार होना चाहिए था। इन्होंने अपनी भूमि को राजा की अनुमति के बिना अपने समर्थकों के बीच बांट देने के अधिकार को भी स्वयं ही ग्रहण कर लिया। इस प्रकार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई जो ज़मीन पर बिना काम किए ही इससे कमाते थे। ऐसी समाज व्यवस्था को ‘सामंतवादी व्यवस्था’ कहा जा सकता है। सामंतवादी समाज की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें ऐसे लोग अधिक शक्तिशाली होते हैं जो ज़मीन पर बिना काम किए उस पर अधिकार रखते हैं।
सामंतो द्वारा लगान वसूली
इस समय के निर्धन लोगों के विषय में कई कहानियाँ मिलती हैं। कई लोग ग़रीबी से तंग आकर डाकू तथा लुटेरे बन जाते थे। जहाँ तक ग्रामों का सवाल है, जिनमें अधिकतर आबादी बसती थी, हमें किसानों के जीवन के बारे में साहित्यिक कृतियों तथा भूमि अनुदान से सम्बन्धित अभिलेखों से पता चलता है। धर्मशास्त्रों के व्याख्याकारों के अनुसार, पहले की तरह लगान की दर अभी भी कुल उत्पादन का छठा हिस्सा थी। लेकिन कुद अनुदानों से हमें पता चलता है कि इसके अलावा भी कई प्रकार के कर थे। जैसे तालाब-कर और चारागाह-कर। किसानों को निर्धारित लगान के अलावा ये कर भी देने पड़ते थे। कुछ अनुदानों से ज़मीन के मालिक को यह अधिकार मिल जाता था कि वह उस ज़मीन पर उचित अथवा अनुचित अर्थात अपनी इच्छा से कर लगा सकता था जो ग़रीब किसानों को लगान के अलावा चुकाना ही पड़ता था। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। मध्य भारत तथा उड़ीसा के कुछ मामलों में तो हम पाते हैं कि मध्ययुगीन यूरोप के कृषि दासों की भाँति यहाँ भी गाँवों के साथ-साथ वहाँ बसे हुए किसान, चरवाहे तथा दस्तकार भी दान में दे दिये जाते थे। साहित्यिक कृतियों में हमें ऐसे सामंतों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो पैसा वसूलने का कोई भी मौक़ा चूकते नहीं थे। बताया जाता है कि राजपूत सरदार तो बटेरों, मृत पक्षियों, सूअर की लीद तथा मृत व्यक्तियों के क़फ़न से भी पैसा बनाया करते थे। एक अन्य सामंत की चर्चा है कि जिसके अत्याचारों से त्रस्त होकर गाँव की सारी की सारी आबादी ने गाँव को ही छोड़ दिया था।
सरदारों के ये अत्याचार तो थे ही फिर इसके ऊपर युद्ध और बाढ़ का प्रकोप भी था। युद्ध में नहरों और तालाबों को तोड़ देना, गाँव के गाँव ही जला देना, ज़बर्दस्ती सारे अनाज और सारे पशुओं को क़ब्ज़े में कर लेना आम बात थी। यहाँ तक कि सामंतवादी व्यवस्था के लेखकों ने इस प्रकार के कार्यों को उचित माना है।
वर्ण व्यवस्था
पहले से चली आ रही वर्ण व्यवस्था इस युग में भी क़ायम रही। स्मृतियों के लेखकों ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर तो कहा ही, शूद्रों की सामाजिक और धार्मिक अयोग्यता को उचित ठहराने में तो वे पिछले लेखकों से कहीं आगे निकल गए। एक लेखक, पराशर के अनुसार शूद्र के साथ भोजन, उसके साथ मिलना-जुलना, शूद्र के साथ एक ही आसन पर बैठना तथा शूद्र से शिक्षा ग्रहण करना ऐसे कार्य हैं जो उच्चतम व्यक्ति का नीच बना देते हैं। यहाँ तक की शूद्रों की छाया तक दूषित थी। यह कहना कठिन है कि स्मृतियों के रचनाकारों के विचारों का व्यावहारिक जीवन में कितना पालन किया जाता था, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि नीची समझी जाने वाली जातियों की इस काल में स्थिति और भी ख़राब हो गयी। अंतर्जातीय विवाह को भी नीची दृष्टि से देखा जाता था। यदि कोई उच्च जाति पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता था तो उसके बच्चों की जाति माँ की जाति के अनुसार तय की जाती थी। इसके विपरीत यदि उच्च कुल की स्त्री नीच कुल के पुरुष से विवाह करती थी तो बच्चे की जाति बाप की जाति से तय की जाती थी। समसामयिक लेखकों ने उस समय की कई जातियों की चर्चा की है। जिनमें कुम्हार, बुनकर, सुनार, संगीतज्ञ, नाई, चमार, ब्याध तथा मछेरे शामिल थे। इनमें से कुछ ने तो अपने रोजग़ार के हिसाब से संघ बना लिए थे, पर उनकी गिनती भी एक जाति के रूप में ही होती थी। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि स्मृति लेखकों ने दस्तकारी को नीच जाति को पेशा माना है। इस प्रकार अधिकतर मज़दूर और भोलों जैसे आदिवासी, अछूतों की श्रेणी में गिने जाने लगे थे।
राजपूतों का उदय
इस युग में हमें एक नयी जाति, राजपूतों की चर्चा भी मिलती है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कई राजपूत अपने को महाभारत के सूर्य वंश और चन्द्र वंश के क्षत्रियों का वंशज मानते थे। कुछ और अपनी उत्पत्ति का स्रोत उस यज्ञ को बताते थे जो ऋषि वसिष्ठ ने आबू पहाड़ पर किया था। किन्तु आबू यज्ञ का उल्लेख हमें पहली बार सोलहवीं शताब्दी में मिलता है। इन कथाओं से हम केवल इतना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभिन्न राजपूत वंशों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से हुई थी। कुछ विद्वान, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, यह मानते हैं कि कुछ राजपूत वंशों की उत्पत्ति उन हूण और सीथियाई लोगों से हुई होगी जोहर्ष के काल के बाद भारत में बस गए। कुछ अन्य वंशों की उत्पत्ति भारतीय क़बीलों से ही हुई। विभिन्न कालों में क्षत्रियों के अलावा ब्राह्मण तथा वैश्य वंशों ने भी शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कालान्तर में शासन करने वाले सभी वंशों को एक जाति का माना जाने लगा और ये ‘राजपुत्र’ अथवा ‘राजपूत’ कहे जाने लगे और क्षत्रिय वंश में शामिल हो गए।
यह स्पष्ट है कि जातियों का वर्गीकरण इतना पक्का नहीं था, जैसा कि आम तौर पर माना जाता है। विभिन्न दल अथवा व्यक्ति उच्च वर्ग की सदस्यता हासिल कर सकते थे, वे नीची जाति में गिर भी सकते थे। इसका एक उदाहरण हमें कायस्थ जाति में मिलता है। जिसका वर्णन सबसे पहले इसी काल में मिलता है। आरम्भ में विभिन्न जातियों, जिनमें ब्राह्मण और शूद्र भी शामिल थे, के ऐसे लोग जो राजघरानों में काम करते थे, उन्हें ‘कायस्थ’ कहा जाता था। कालान्तर में इन्हीं की एक विशिष्ट जाति बन गई। इस काल में हिन्दू धर्म का प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ। कई बौद्ध और जैनियों के अलावा कई विदेशी तथा भारतीय क़बीले हिन्दू धर्म में एकात्म हो गए। समय के साथ नये वर्गों ने, विभिन्न जातियों और उपजातियों का रूप धारण कर लिया। पर उन्होंने विवाह, अपने विशिष्ट देवी-दवताओं की पूजा तथा अन्य त्योहारों को मनाना जारी रखा। इस प्रकार धर्म और समाज व्यवस्था अधिक जटिल होती चली गई।
नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा,बिहार
बौद्ध विहार
उच्च शिक्षा में धार्मिक विषयों के अलावा अन्य विषय भी शामिल थे, और इसका केन्द्र बौद्ध विहार ही था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध, बिहार का नालन्दा विश्वविद्यालय था। अन्य शिक्षा के प्रमुख केन्द्र विक्रमशिला और उद्दंडपुर थे। ये भी बिहार में ही थे। इन केन्द्रों में दूर-दूर से, यहाँ तक की तिब्बत से भी, विद्यार्थी आते थे। यहाँ शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाती थी। इन विश्वविद्यालयों का खर्च शासकों द्वारा दी गई मुद्रा और भूमि के दान से चलता था। नालन्दा को दो सौ ग्रामों का अनुदान प्राप्त था।
शिक्षा का एक अन्य प्रमुख केन्द्र कश्मीर था। इस काल में कश्मीर में शैव मत तथा अन्य मतावलंबी शिक्षा केन्द्र थे। दक्षिण भारत में मदुरई तथा श्रृंगेरी में भी कई महत्त्वपूर्ण मठों की स्थापना हुई। इन केन्द्रों में प्रमुख रूप से धर्म तथा दर्शन शास्त्र पर विचार-विमर्श होता था। भारतके विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मठों और शिक्षा केन्द्रों के कारण विचार विनिमय आसानी और शीघ्रता से देश के एक भाग से दूसरे भाग तक हो सकते थे। किसी दर्शन शास्त्री की विद्या उस समय तक पूर्ण नहीं मानी जाती थी जब तक वह देश के विभिन्न भागों में जाकर वहाँ के लोगों से शास्त्रार्थ न करता हो। इस तरह देश में विचारों के मुक्त और शीघ्रतापूर्ण आदान-प्रदान से भारत की सांस्कृतिक एकता को बहुत बल मिला, लेकिन इसके बावजूद इस काल में शिक्षित वर्ग का दृष्टिकोण अधिक संकीर्ण होता गया। वे नये विचारों का प्रतिपादन अथवा उसका स्वागत करने के स्थान पर केवल अतीत के ज्ञान पर ही निर्भर करते थे। वे भारत के बाहर पनपने वाले वैज्ञानिक विचारों से भी स्वयं को अलग रखते थे। इस प्रवृत्ति की झलक हमें मध्य एशिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विद्वान अलबेरूनी की रचनाओं में मिलती है। अलबेरूनी ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में क़रीब दस वर्षों तक भारत में रहा। यद्यपि वह भारतीय ज्ञान और विज्ञान का प्रशंसक था, उसने यहाँ के शिक्षित वर्गों और विशेषकर ब्राह्मणों की संकीर्णता की चर्चा भी की हैः- ‘ये घमण्डी, गर्वीले, दंभी तथा संकीर्ण प्रवृत्ति के हैं। ये प्रवृत्ति से ही अपने ज्ञान को दूसरों को बाँटने के मामले में कंजूस हैं और इस बात का अधिक से अधिक ख्याल रखते हैं कि कहीं और कोई जात के किसी आदमी, विशेषकर किसी विदेशी को उनका ज्ञान नहीं मिल जाए। उनका विश्वास है कि उनके अलावा और किसी को भी विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है।’ ज्ञान को ही कुछ लोगों तक सीमित रखने की उनकी इस प्रवृत्ति तथा घमण्ड के कारण तथा किसी और स्रोत से प्राप्त ज्ञान को तुच्छ समझने के कारण भारतवर्ष इस मामले में पिछड़ गया। कालान्तर में उसे इस प्रवृत्ति का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा।
धार्मिक विचार
इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का ह्रास हुआ, यद्यपि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रभाव दसवीं शताब्दी तक बना रहा। इसी काल में बौद्ध धर्म अपने जन्म के देश में समाप्त प्रायः हो गया पर हिन्दू धर्म का पुर्नजागरण और उसका विस्तार हुआ। इसने अनेकों रूप अपनाए जिसमें सबसे प्रमुख शिव और विष्णु की लोकप्रियता थी। इन देवों की पूजा को प्रमुख मानते हुए कई सम्प्रदाय उठ खड़े हुए पर बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों को चुनौती दी गई।
कालान्तर में शिव तथा विष्णु प्रमुख देवता बन गए और सूर्य, ब्रह्मा आदि की लोकप्रियता कम हो गई। पूर्वी भारत में पूजा की एक नई विधि का विकास हुआ। यह शक्ति पूजा थी जिसमें स्त्री शक्ति को सृष्टि का आधार सिद्धांत माना गया। इस प्रकार बौद्धों ने अतीत के बोधिसत्वों की पत्नी के रूप में तारा तथा हिन्दुओं नेदुर्गा और काली की पूजा शुरू की, जिन्हें शिव की पत्नियाँ बताया गया।
इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव पूर्वी भारत तक सीमित रहा। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। दसवीं शताब्दी के बाद उनके पतन से बौद्ध धर्म को भी धक्का पहुँचा। लेकिन इससे ज़्यादा गम्भीर बौद्ध धर्म के आंतरिक मतभेद थे। बुद्ध ने स्वयं एक व्यावहारिक दर्शन का प्रसार किया था। जिसमें पुजारी वर्ग की भूमिका न्यूनतम थी तथा ईश्वर तथा उसके अस्तित्व के बारे में अधिक अटकलबाज़ी की गुंजाइश नहीं थी। ईस्वीं युग के आरम्भ की शताब्दियों में महायान मत का विकास हुआ, जिसमें बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। धीरे-धीरे इनकी पूजा परिपाटी और जटिल तथा भव्य होती गई। साथ-साथ यह विश्वास मज़बूत होता गया कि पूजक मंत्रों को पढ़कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उनका यह भी विश्वास था कि इन कार्यकलापों तथा विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने से उन्हें हवा में उड़ने और अद्श्य होने जैसी दैवी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती थीं। मनुष्य इस प्रकार से प्रकृति पर नियंत्रण के लिए हमेशा से इच्छुक रहा है, पर इसकी ये इच्छाएँ केवल आधुनिक विज्ञान के विकास से पूरी हुई है। कई हिन्दू योगियों ने भी इस प्रकार की चेष्टा की। इनमें सबसे प्रसिद्ध गोरखनाथ थे। गोरखनाथ शिष्यों को नाथपंथी कहा जाता है तथा एक समय ये सारे उत्तर भारत में लोकप्रिय थे। इनमें से कई योगी नीची जाति के थे और उन्होंने वर्ण-व्यवस्था तथा ब्रह्मणों के विशेषाधिकार की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तन्त्र कहा जाता है और इसकी सदस्यता बिना जातिभेद के सभी के लिए खुली थी।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का पतन नहीं हुआ, लेकिन उसने कई ऐसे रूप धारण कर लिए जो हिन्दू धर्म से बहुत भिन्न नहीं थे।
जैन धर्म
पश्चिम भारत में, विशेषकर व्यापारी वर्ग के बीच, जैन धर्म लोकप्रिय बना रहा। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को प्रोत्साहित किया। उन्हीं के काल में आबू पहाड़ पर दिलवाड़ा जैसे भव्य मन्दिरों का निर्माण किया गया। मालवा के परमार शासकों ने भी जैन तीर्थंकरों और महावीर की, बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ बनवायी जिन्हें अब ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े-बड़े जैनालय बनवाए, जो यात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में लोकप्रिय हुए।
दक्षिण भारत में जैन धर्म नौवीं और दसवीं शताब्दियों में शिखर पर पहुँच गया। कर्नाटक के गंग शासक जैन धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। इस काल में विभिन्न हिस्सों में जैन मन्दिरों तथा महास्तम्भों का निर्माण किया गया। श्रावण बेलगोला में महावीर की विशाल प्रतिमा भी इसी काल में बनी। यह मूर्ति 18 मीटर ऊँची तथा एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई है। इसमें महावीर को तपस्या की मुद्रा में खड़ा दिखाया गया है। वे अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पांवों में साँप लिपटे हुए हैं तथा चीटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। जैनियों के चार वरों (शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास) के सिद्धांत ने लोगों के बीच जैन धर्म को लोकप्रिय बना दिया था। कालान्तर में जैनियों की संकीर्णता तथा राजसी प्रोत्साहन की कमी से धीरे-धीरे इसका भी ह्रास होता गया। इसके अलावा इसी काल में दक्षिण भारत में शिव तथा विष्णु से सम्बन्धित कई लोकप्रिय आन्दोलन शुरू हो गए। जिसके कारण जैनियों की लोकप्रियता घटती चली गई। इनमें से सबसे प्रमुख भक्ति आन्दोलन था। जिसका नेतृत्व लोकप्रिय सन्तों ने किया, जिन्हें ‘नयनार’ तथा ‘अलवार’ पुकारा जाता था। इनके मत में कठोर तपस्या का कोई स्थान नहीं था। वे धर्म को रीति-रिवाजों से जटिल पूजा, तथा केवल सिद्धांत मात्र नहीं मानते थे। इनके अनुसार धर्म ईश्वर तथा भक्त के बीच एक जीवन्त सम्पर्क साधन था। ये सन्त तमिल और तेलुगु में लिखते थे, जिन्हें सभी समझ सकते हों। ये सन्त जगह-जगह स्वयं जाकर लोगों को भक्ति और प्रेम के सिद्धांत बताते थे। इनमें से कुछ नीची जाति के थे, पर कुछ ब्राह्मण भी थे। इनके अलावा इस आन्दोलन में कुछ स्त्रियाँ भी थीं। क़रीब-क़रीब सभी सन्तों ने जाति व्यवस्था का विरोध किए बिना उससे उससे उत्पन्न होने वाले भेदभाव को ग़लत बताया। नीची जाति के लोगों को वैदिक ज्ञान तथा पूजा से बहिष्कृत किया गया, लेकिन इन सन्तों द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग सभी के लिए खुला था, उसमें जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था।
भक्ति आंदोलन और कथा-कहानियाँ
भक्ति आंदोलन ने न केवल कई बौद्ध तथा जैन मताबलम्बियों को हिन्दू धर्म की ओर आकर्षित किया, वरन उन कई क़बीलों को भी हिन्दू धर्म में मिल जाने को प्रेरित किया, जो अब तक इसके बाहर थे। इस प्रकार विभिन्न क़बीले जाति व्यवस्था में ढलकर हिन्दू बन गए थे। आम तौर पर वे अपने क़बीलाई देवी-देवताओं की ही पूजा करते थे, लेकिन बाद में उन्हें शिव तथा विष्णु के मित्र अथवा पत्नियाँ बना दिया गया। इस प्रकार के सांस्कृतिक सम्मेलन में कथा-कहानियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वैदिक परंपरा
बारहवीं शताब्दी के दौरान एक और लोकप्रिय आंदोलन शुरू हुआ। जिसे लिंगायत कहते हैं। इसके प्रतिष्ठाता ‘बसव’ और उनका भतीजा ‘चन्नबसव’ थे, जो कर्नाटक के कलचूरी नरेशों के दरबार में रहते थे। इन्होंने जैन मतावलम्बियों से कड़े विरोध के बाद इस मत की स्थापना की। लिंगायत शिव के पूजक होते हैं। इन्होंने जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, तथा उपवास, बलि प्रथा औरतीर्थों का बहिष्कार किया। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह की स्वीकृति दी। इस प्रकार दक्षिण तथा उत्तर भारत, दोनों स्थानों में हिन्दू धर्म के विस्तार और पुनर्जागरण ने दो रूप अपनाए –
1. एक ओर वेदों तथा वैदिक पूजा और उनके साथ-साथ साहित्य तथा बौद्धिक आंदोलनों पर ज़ोर दिया गया।
2. दूसरी ओर उत्तर भारत में तंत्र तथा दक्षिण भारत में भक्ति जैसे लोकप्रिय आंदोलनों का आरम्भ हुआ। तंत्र तथा भक्ति के आंदोलनों में जाति-भेद का कोई स्थान नहीं था और इनके द्वार सब के लिए खुले थे।
बौद्धिक स्तर पर बौद्ध तथा जैन धर्म को सबसे बड़ी चुनौती शंकर ने दी, जिन्होंने हिन्दू दर्शन की पुनःव्याख्या की। शंकर का जन्म सम्भवतः नौवीं शताब्दी में केरल में हुआ था। उनके प्रारम्भिक जीवन के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है तथा उनके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हो गई हैं। कहा जाता है कि जैन मतावलम्बियों के विरोध के कारण उन्हें मदुरई से भागना पड़ा और उसके बाद उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की तथा शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े विरोधियों को पराजित किया। जब वे मदुरई लौटे तब वहाँ के नरेश ने उनका भव्य स्वागत किया तथा अपने दरबार से जैनियों को निकाल दिया।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि शंकर को अपने सिद्धांत प्रतिपादित करने के दौरान बौद्ध तथा जैन मतावलम्बियों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार ईश्वर तथा उसकी सृष्टि वास्तव में एक है। उसके अनुसार मोक्ष का मार्ग इसी बात की अनुभूति थी कि ईश्वर तथा उसकी सृष्टि एक ही है। इस दर्शन को वेदान्त कहा जाता है। इस प्रकार शंकर ने वेदों को उच्चतम ज्ञान का स्रोत बताया। शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान का मार्ग कुछ ही लोगों की समझ में आ सकता था। इससे जनसमूह प्रभावित नहीं हो सकता था। ग्यारहवीं शताब्दी में एक और प्रसिद्ध विद्वान रामानुज ने भक्ति तथा वेदों की परम्परा के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार मोक्ष के लिए ईश्वर के ज्ञान से अधिक उसकी कृपादृष्टि आवश्यक थी। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसके द्वार बिना जाति भेद के खुले थे। इस प्रकार रामानुज ने भक्ति के लोकप्रिय आंदोलन तथा वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच सेतु का कार्य किया। रामानुज के कई बौद्धिक अनुयायी हुए। इनमें मध्वाचार्य (चौदहवीं शताब्दी) तथा उत्तर भारत में रामानन्द (पंद्रहवीं शताब्दी) प्रमुख हैं। इस प्रकार आठवीं और बारहवीं शताब्दियों के बीच के काल में न केवल समाज में वरन धार्मिक विचारों में भी अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए।
भारत के राज्यों की संस्कृति
अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति
अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के लोगों की अपनी-अपनी अलग पगड़ी एवं परिधान है।
बुनाई कला का अपना महत्त्व है एवं हर जनजाति की अपनी विशिष्ट शैली है।
नृत्य सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है।
लोसर, मेपिन एवं सोलुंग यहाँ के प्रमुख जनजातीय पर्व है।
असम की संस्कृति
नागारिक विमानों की नियमित उड़ानें गोपीनाथ बाड़दोलाई हवाई अड्डा (गुवाहाटी), सलोनीबाड़ी (तेजपुर), मोहनबाड़ी (उत्तरी लखीमपुर), कुंभीरग्राम (सिलचर), और रोवरियाह (जोरहाट) से होती हैं।
असम में अनेक रंगारंग त्योहार मनाए जाते हैं। ‘बिहू’ असम का मुख्य पर्व है।
यह वर्ष में तीन बार मनाया जाता है- ‘रंगाली बिहू’ या ‘बोहाग बिहू’ फ़सल की बुआई की शुरुआत का प्रतीक है।
आंध्र प्रदेश की संस्कृति
भारतीय सांस्कृतिक विरासत में आंध्र प्रदेश का योगदान उल्लेखनीय है। प्राचीन समय से इस क्षेत्र में वास्तुकला औरचित्रकला अत्यंत विकसित रही। भारतीय परंपरा में कुचिपुडी नृत्य शैली अनोखी है। कर्नाटक (दक्षिण भारतीय) संगीत ने आंध्र प्रदेश से बहुत कुछ ग्रहण किया है। कई दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीतकार आंध्र प्रदेश के हैं और बहुत सी संगीत रचनाओं की भाषा तेलुगु रही है। द्रविड़ परिवार की चार प्रमुख साहित्यिक भाषाओं में से एक तेलुगु का भारतीय भाषाओं में सम्मानित स्थान है।
उत्तर प्रदेश की संस्कृति
उत्तर प्रदेश हिन्दुओं की प्राचीन सभ्यता का उदगम स्थल है।
वैदिक साहित्य महाकाव्य रामायण और महाभारत[6] के उल्लेखनीय हिस्सों का मूल यहाँ के कई आश्रमों में है। बौद्ध-हिन्दू काल[7] के ग्रन्थों व वास्तुशिल्प ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत में बड़ा योगदान दिया है। 1947 के बाद से भारत सरकार का चिह्न मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए चार सिंह युक्त स्तम्भ[8] पर आधारित है।
वास्तुशिल्प, चित्रकारी, संगीत, नृत्यकला और दो भाषाएँ[9] मुग़ल काल के दौरान यहाँ पर फली-फूली। इस काल के चित्रों में सामान्यतया धार्मिक व ऐतिहासिक ग्रन्थों का चित्रण है। यद्यपि साहित्य व संगीत का उल्लेख प्राचीनसंस्कृत ग्रन्थों में किया गया है और माना जाता है कि गुप्त काल (लगभग 320-540) में संगीत समृद्ध हुआ। संगीत परम्परा का अधिकांश हिस्सा इस काल के दौरान उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ। तानसेन व बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञमुग़ल शहंशाह अकबर के दरबार में थे, जो राज्य व समूचे देश में आज भी विख्यात हैं। भारतीय संगीत के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य, सितार[10] और तबले का विकास इसी काल के दौरान इस क्षेत्र में हुआ। 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश मेंवृन्दावन व मथुरा के मन्दिरों में भक्तिपूर्ण नृत्य के तौर पर विकसित शास्त्रीय नृत्य शैली कथक उत्तरी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय गीत व नृत्य भी हैं। सबसे प्रसिद्ध लोकगीत मौसमों पर आधारित हैं।
उत्तराखण्ड की संस्कृति
उत्तराखण्ड राज्य के अधिकांश त्योहार और अवकाश हिन्दू पंचांग पर आधारित हैं। उत्तराखण्ड के कुछ महत्त्वपूर्ण हिन्दू त्योहारों और अवकाशों में बुराई के प्रतीक रावण पर राम की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला दशहरा; धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित दीपावली; भगवान शिव की आराधना का दिन शिवरात्रि; रंगों का त्योहार होली और भगवानकृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी शामिल हैं। अल-हुसैन बिन अली का शहीदी दिवसमुहर्रम; उपवास (रोज़े) रखने का महीना रमज़ान; और धर्म वैधानिक त्योहार ईद राज्य में मनाए जाने वाले मुसलमानोंके कुछ प्रमुख त्योहारों में से हैं।
ओडिशा की संस्कृति
ओडिशा की समृद्ध कलात्मक विरासत है और इसने भारतीय कला एवं वास्तुशिल्प के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों का सृजन किया है। भित्तिचित्रों पत्थर व लकड़ी पर नक़्क़ाशी देव चित्र[11] और ताड़पत्रों पर चित्रकारी के माध्यम से कलात्मक परंपराएं आज भी क़ायम हैं। हस्तशिल्प कलाकार चांदी में बेहद महीन जाली की कटाई की अलंकृत शिल्प कला के लिए विख्यात हैं।
कर्नाटक की संस्कृति
कर्नाटक में विभिन्न राजवंशों के योगदान के कारण एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मौजूद है, जिसमें विभिन्न धर्मों और दर्शनों को बढ़ावा दिया गया है।
इन्होंने साहित्य वास्तुशिल्प, लोकगीतों, संगीत, चित्रकला और लघु कलाओं पर अपना प्रभाव छोड़ा है।
मैसूर से 90 किमी. दूर श्रवणबेलगोला नगर में मौर्य वास्तुशिल्प और मूर्तिशिल्प के उल्लेखनीय उदाहरण मिलते हैं, जैसे जैन मुनि बाहुबली (गोमतेश्वर) की लगभग 1,000 वर्ष पुरानी मानी जाने वाली विशालकाय प्रस्तर प्रतिमा।
केरल की संस्कृति
केरल की संस्कृति वास्तव में भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप की तरह केरल की संस्कृति का भी एक पुरातन इतिहास है जो अपने आप में महत्त्वपूर्ण होने का दावा करता है। केरल की संस्कृति भी एक समग्र और महानगरीय संस्कृति है जिसमें कई लोगों और जातियों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। केरल के लोगों के बीच समग्र और विविधतावादी सहिष्णुता और दृष्टिकोण की उदारता की भावना का उद्वव अभी है जिससे नेतृत्व संस्कृति का विकास लगातार जारी है।
गुजरात की संस्कृति
गुजरात की अधिकांश लोक संस्कृति और लोकगीत हिन्दू धार्मिक साहित्य पुराण में वर्णित भगवान कृष्ण से जुड़ी किंवदंतियों से प्रतिबिंबित होती है। कृष्ण के सम्मान में किया जाने वाला रासनृत्य और रासलीला प्रसिद्ध लोकनृत्य “गरबा” के रूप में अब भी प्रचलित है। यह नृत्य देवी दुर्गा के नवरात्र पर्व में किया जाता है। एक लोक नाट्य भवई भी अभी अस्तित्व में है।
गुजरात में शैववाद के साथ-साथ वैष्णववाद भी लंबे समय से फलता-फूलता रहा है, जिनसे भक्ति मत का उद्भव हुआ। प्रमुख संतों, कवियों और संगीतज्ञों में 15वीं सदी में पदों के रचयिता नरसी मेहता, अपने महल को त्यागने वाली 16वीं सदी की राजपूत राजकुमारी व भजनों की रचनाकार मीराबाई, 18वीं सदी के कवि और लेखक प्रेमानंद और भक्ति मत को लोकप्रिय बनाने वाले गीतकार दयाराम शामिल हैं। भारत में अन्य जगहों की तुलना में अहिंसा और शाकाहार की विशिष्टता वाले जैन धर्म ने गुजरात में गहरी जड़े जमाई। ज़रथुस्त्र के अनुयायी पारसी 17वीं सदी के बाद किसी समय फ़ारस से भागकर सबसे पहले गुजरात के तट पर ही बसे थे।
गोवा की संस्कृति
सुरम्य सागरतट पर बसा गोवा प्रांत अपनी प्राकृतिक सुंदरता व अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है।
आज़ादी से पहले यह प्रांत पुर्तग़ीज व फ्रांसीसियों का उपनिवेश रह चुका है।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति
छत्तीसगढ़ की संस्कृति की एक धारा लोक जीवन में प्रवाहित है ।
यह धारा जीवन के उल्लास से रसमय है और अनेक रुपों में प्रकट है।
इसके अंतर्गत अंचल के प्रसिद्ध उत्सव, नृत्य- संगीत, मेला-मड़ई, तथा लोक शिल्प शामिल है।
जम्मू और कश्मीर की संस्कृति
आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण पर राम की विजय के प्रतीक रूप में दशहरा या वियजदशमी का त्योहार मनाया जाता है।
शिवरात्रि भी जम्मू और कश्मीर में श्रद्धा और भाक्ति के साथ मनाई जाती है।
राज्य में मनाए जाने वाले चार मुस्लिम त्योहार हैं- ईद-उल-फितर, ईद उल ज़ुहा, ईद-ए-मिलाद या मीलादुन्नबी और मेराज आलम। मुहर्रम भी मनाया जाता हैं।
झारखण्ड की संस्कृति
झारखण्ड के सांस्कृतिक क्षेत्र अपने-अपने भाषाई क्षेत्रों से जुड़े हैं।
हिन्दी, संथाली, मुंडा, हो, कुडुख, मैथिली, माल्तो, कुरमाली, खोरठा और उर्दू भाषाएँ यहाँ पर बोली जाती है।
भोजपुरी बोली का लिखित साहित्य न होने के बावजूद इसका उल्लेखनीय मौखिक लोक साहित्य है।
मगही की भी समृद्ध लोक परम्परा है।
तमिलनाडु की संस्कृति
फ़सल कटाई के त्योहार पोंगल में जनवरी माह में किसान अपनी अच्छी फ़सल के लिए आभार प्रकट करने हेतु सूर्य,पृथ्वी और पशुओं की पूजा करते हैं। पोंगल के बाद दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ‘जल्लीकट्टू’[12] होता है। तमिलनाडु में अलंगनल्लूर ‘जल्लीकट्टू’ के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। ‘चित्तिरै’ मदुरै का लोकप्रिय त्योहार है। यह पांडय राजकुमारी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के अलैकिक परिणय बंधन का समृति में मनाया जाता है। तमिल महीने ‘आदि’ के अठारहवें दिन नदियों के किनारे ‘आदिपेरूकु’ पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही नई फ़सल की बुवाई से संबंधित काम भी शुरू हो जाता है।
त्रिपुरा की संस्कृति
त्रिपुरा में निम्नलिखित त्योहार मनाये जाते है-
तीर्थमुख और उनाकोटी में मकर संक्रांति
होली
उनोकोटी, ब्रहाकुंड (मोहनपुर) में अशोकाष्टमी
राश
बंगाली नववर्ष
गारिया, धामेल, बिजू और होजगिरि उत्सव
नौका दौड़ और मनसा मंगल उत्सव
दिल्ली की संस्कृति
दिल्ली की संस्कृति यहाँ के लम्बे इतिहास और भारत की राजधानी के रूप में ऐतिहासिक स्थिति से पूर्ण प्रभावित रही है, यह शहर में बने कई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों से ज्ञात है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने दिल्लीशहर में लगभग 1200 धरोहर स्थल घोषित किए हैं, जो कि विश्व में किसी भी शहर से कहीं अधिक है। महानगर होने की वजह से दिल्ली में भारत के सभी प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं।
नागालैंड की संस्कृति
नागालैंड में जनजातीय संगठन में कोल्याक के निरंकुश अंग (सरदार) और सेमा व चांग के आनुवंशिक मुखिया से लेकर अंगामी, आओ, ल्होरा और रेंगमा की लोकतांत्रिक संरचनाओं जैसी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। मोरुंग[13] गाँव का प्रमुख संस्थान होता है, जहाँ पहले खोपड़िया और युद्ध के अन्य विजय चिह्न टांगे जाते थे। इनके स्तम्भों पर अब भी बाघ, धनेश, मानव तथा अन्य आकृतियों की नक़्क़ाशी की जाती है। नागा समाज में महिलाओं को अपेक्षाकृत ऊँचा और सम्मानजनक स्थान प्राप्त है।
पंजाब की संस्कृति
लोकगीत, प्रेम और युद्ध के नृत्य मेले और त्योहार, नृत्य, संगीत तथा साहित्य इस राज्य के सांस्कृतिक जीवन की विशेषताएं हैं। पंजाबी साहित्य की उत्पत्ति को 13 वीं शताब्दी के मुसलमान सूफी संत शेख़ फरीद के रहस्यवादी और धार्मिक दोहों तथा सिक्ख पंथ के संस्थापक, 15वीं-16वीं शताब्दी के गुरु नानक से जोड़ा जा सकता है। जिन्होंने पहली बार काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में व्यापक रुप से पंजाबी भाषा का उपयोग किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पंजाबी साहित्य को समृद्ध बनाने में वारिस शाह की भूमिका अतुलनीय है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कवि व लेखन भाई वीरसिंह तथा कवि पूरण सिंह और धनी राम चैत्रिक के लेखन के साथ ही पंजाबी साहित्य ने आधुनिक काल में प्रवेश किया।
पश्चिम बंगाल की संस्कृति
बंगालियों ने हमेशा से ही साहित्य, कला, संगीत और रंगमंच (नाटक) को संरक्षण दिया है। बांग्ला साहित्य का आविर्भाव 12वीं सदी से पहले हुआ। हिन्दू धर्म के एक संघन भावनात्मक स्वरूप, चैतन्य आन्दोलन, को मध्यकालीनसंत चैतन्य (1485-1533) ने प्रेरित किया, जिसने 19वीं सदी के आरम्भ तक बांग्ला कविता के परवर्ती विकास को आकार दिया। इसके बाद पश्चिम के साथ हुए सम्पर्क ने एक द्रुत बहुमुखी सृजनात्मक युग की शुरुआत की। आधुनक युग में अन्य साहित्यकारों के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रबीन्द्रनाथ ठाकुर (1861-1941) हुए, जिनका योगदान आज भी भारतीय साहित्यिक परिदृश्य पर छाया हुआ है।
बिहार की संस्कृति
बिहार का सांस्कृतिक क्षेत्र भाषाई क्षेत्र के साथ क़रीबी सम्बन्ध दर्शाता है। मैथिली प्राचीन मिथिला (विदेह, वर्तमान तिरहुत) की भाषा है, जिसमें ब्राह्मणवादी जीवन व्यवस्था की प्रधानता है। मैथिली बिहार की एकमात्र बोली है, जिसकी अपनी लिपि (तिरहुत) और समृद्ध साहित्यिक इतिहास है। मैथिली के प्राचीनतम और सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकारों में विद्यापति अपने शृंगारिक व भक्ति गीतों के लिए विख्यात हैं।
मणिपुर की संस्कृति
मणिपुर में वर्ष भर त्योहार मनाए जाते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं होता जब कोई त्योहार न मनाया जाता हो। त्योहार मणिपुर के निवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। राज्य के प्रमुख त्योहार है-
लाई हारोबा
रासलीला
चिरओबा
निंगोल चाक-कुबा
मध्य प्रदेश की संस्कृति
मध्य प्रदेश में अनेक मन्दिर, क़िले व गुफ़ाएँ हैं, जिनमें क्षेत्र के पूर्व इतिहास और स्थानीय राजवंशों व राज्यों, दोनों के ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से रोमांचक प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के प्रारम्भिक स्मारकों में से एक सतना के पास भरहुत का स्तूप (लगभग 175 ई.पू.) है, जिसके अवशेष अब कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालयमें रखे हैं। ऐसे ही एक स्मारक, साँची के स्तूप] को मूलत: 265 से 238 ई.पू. में सम्राट अशोक ने बनवाया था। बाद में शुंग राजाओं ने इस स्तूप में और भी काम करवाया। बौद्ध विषयों पर आधारित चित्रों से सुसज्जित महू के समीप स्थित बाघ गुफ़ाएँ विशेषकर उल्लेखनीय हैं। विदिशा के समीप उदयगिरि की गुफ़ाएँ (बौद्ध और जैन मठ) चट्टान काटकर बनाए गए वास्तुशिल्प और कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।
महाराष्ट्र की संस्कृति
महाराष्ट्र का सांस्कृतिक जीवन प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभावों का मिश्रण है। मराठी भाषा और मराठी साहित्य का विकास महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है। स्थानीय व क्षेत्रीय देवताओं के प्रति भक्ति, ज्ञानेश्वर व तुकाराम जैसे संत कवियों की शिक्षाओं और छत्रपति शिवाजी व अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं के प्रति आदरभाव, महाराष्ट्र की संस्कृति की विशेष पहचान है। कोल्हापुर, तुलजापुर, पंढरपुर, नासिक,अकोला, फल्तन, अंबेजोगाई और चिपलूण व अन्य धार्मिक स्थलों पर दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। मेलों और त्योहारों का भी महत्व कम नहीं है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में गणेश चतुर्थी, रामनवमी, अन्य स्थानीय व क्षेत्रीय मेले और त्योहार महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके द्वारा लोगों का स्थानीय तथा क्षेत्रीय मेल-मिलाप होता है और ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। अन्ध धर्मों के त्योहारों में भी लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, जो सांस्कृतिक जीवन के महानगरीय चरित्र को दर्शाता है। ‘महानुभाव मत’ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा पुनर्जीवित किए गए बौद्ध धर्म से सांस्कृतिक जीवन को नया आयाम मिला है।
मिज़ोरम की संस्कृति
मिज़ो नागरिक मूलत: किसान हैं।
अत: उनकी तमाम गतिविधियां तथा त्योहार भी जंगल की कटाई करके की जाने वाली झूम खेती से ही जुड़े हुए हैं।
मेघालय की संस्कृति
यह क्षेत्र जनजातीय संस्कृति और लोक परम्परा से समृद्ध है। भैंस के सींगों, बाँसुरी और मृदंगों से निकली स्वर लहरियों के साथ नृत्य और मदिरापान यहाँ के सामाजिक समारोहों व धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग है। विवाह सम्बन्ध अपने कुल-गोत्र के बाहर होते हैं। 19वीं सदी के मध्य में ईसाईयत के आगमन और उसके साथ जुड़ी सख़्त नैतिकता ने अनेक जनजातीय और सामुदायिक संस्थाओं को क्षति पहुँचाई है। गारो जाति के लोगों में एक विचित्र प्रथा यह है कि शादी के बाद सबसे छोटा दामाद अपने सास-ससुर के घर आकर रहने लगता है और उसकी सास के मायके में उसके ससुर का प्रतिनिधि नोकरोम बन जाता है। यदि ससुर की मौत हो जाती है तो, नोकरोम की उसकी विधवा सास की शादी कर दी जाती और इस तरह वह माँ और बेटी, दोनों का पति बन जाता है। यह रिवाज अब ख़त्म होता जा रहा है। ख़ासियों में पहले नरबलि की प्रथा भी थी।
राजस्थान की संस्कृति
राजस्थान में मुश्किल से कोई महीना ऐसा जाता होगा, जिसमें धार्मिक उत्सव न हो। सबसे उल्लेखनीय व विशिष्ट उत्सव गणगौर है, जिसमें महादेव व पार्वती कीमिट्टी की मूर्तियों की पूजा 15 दिन तक सभी जातियों की स्त्रियों के द्वारा की जाती है, और बाद में उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन की शोभायात्रा में पुरोहित व अधिकारी भी शामिल होते हैं व बाजे-गाजे के साथ शोभायात्रा निकलती है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। इन अवसरों पर उत्साह व उल्लास का बोलबाला रहता है।
सिक्किम की संस्कृति
सिक्किम के नागरिक भारत के सभी प्रमुख हिन्दू त्योहार दीपावली और दशहरा मनाते हैं।
बौद्ध धर्म के ल्होसार, लूसोंग, सागा दावा, ल्हाबाब ड्युचेन, ड्रुपका टेशी और भूमचू वे त्योहार हैं जो मनाये जाते हैं।
सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भोटिया, लेप्चा और नेपाली समुदायों के लोग हैं।
हिमाचल प्रदेश की संस्कृति
हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से हिन्दी, काँगड़ी, पहाड़ी, पंजाबी, तथा डोगरी आदि भाषाऐं बोली जाती हैं।
हिन्दू, बौद्ध और सिक्ख आदि यहाँ के प्रमुख धर्म हैं।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, मण्डी ऊपरी क्षेत्र किन्नौर, शिमला इत्यादि जनपदों में नाटी नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है।
हरियाणा की संस्कृति
हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन में राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अवसरों की लय प्रतिबिंबित होती है और इसमें प्राचीन भारत की परंपराओं व लोककथाओं का भंडार है। हरियाणा की एक विशिष्ट बोली है और उसमें स्थानीय मुहावरों का प्रचलन है। स्थानीय लोकगीत और नृत्य अपने आकर्षक अंदाज़ में राज्य के सांस्कृतिक जीवन को प्रदर्शित करतें हैं। ये ओज से भरे हैं और स्थानीय संस्कृति की विनोदप्रियता से जुड़े हैं। वसंत ॠतु में मौजमस्ती से भरे होली के त्योहार में लोग एक-दूसरे पर गुलाल उड़ाकर और गीला रंग डालकर मनाते हैं, इसमें उम्र या सामाजिक हैसियत का कोई भेद नहीं होता। भगवान कृष्ण के जन्मदिन, जन्माष्टमी का हरियाणा में विशिष्ट धार्मिक महत्त्व है, क्योंकि कुरुक्षेत्र ही वह रणभूमि थी, जहां कृष्ण ने योद्धा अर्जुन को भगवद्गीता का उपदेश दिया था।
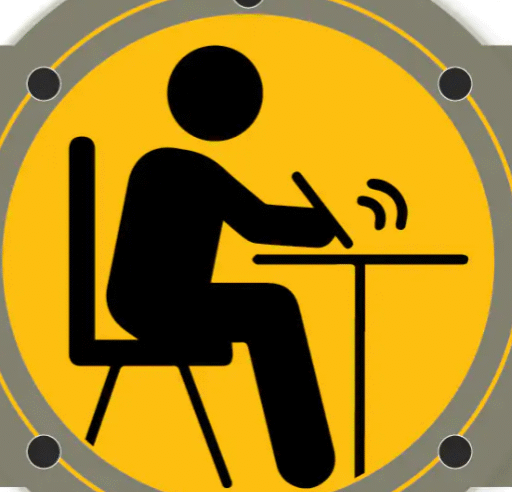












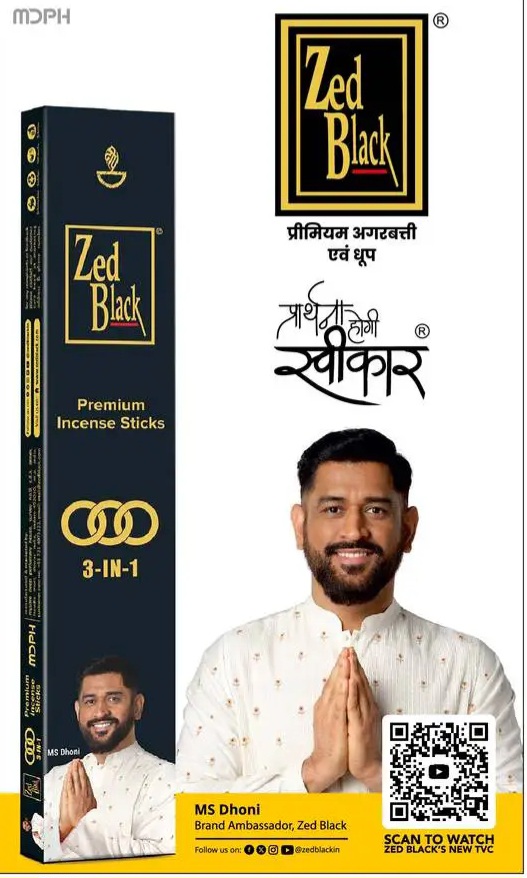
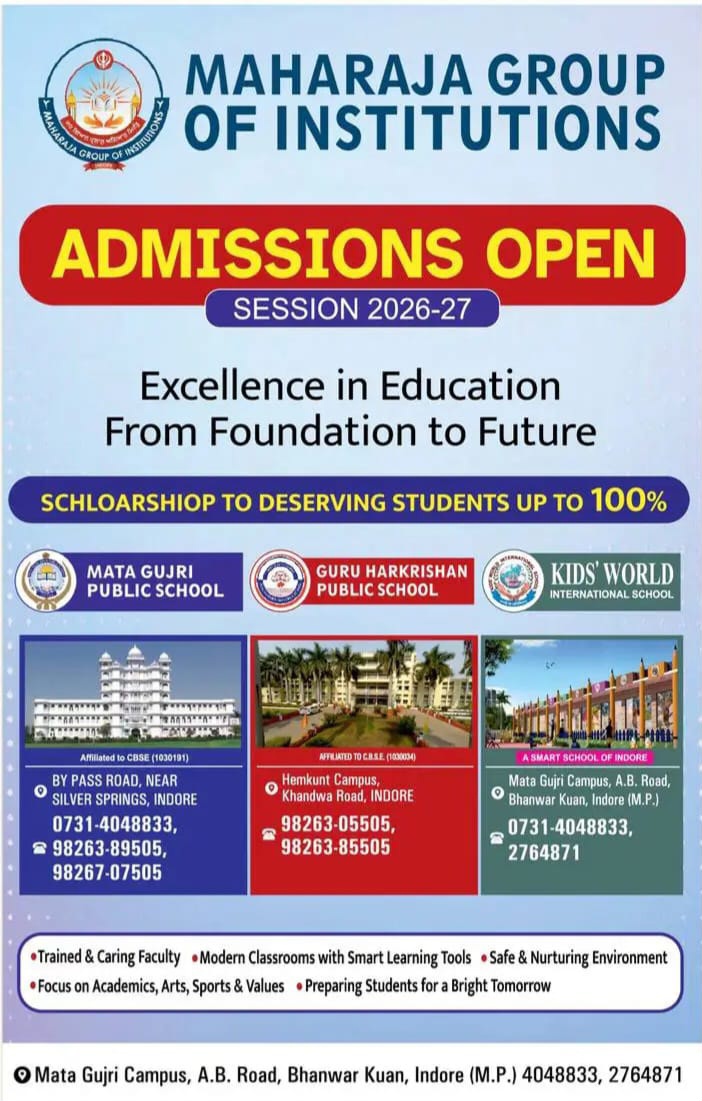


 +91-94068 22273
+91-94068 22273 
