क्लाउड सीडिंग: बादलों को बरसाने की तकनीक
क्लाउड सीडिंग: बादलों को बरसाने की तकनीक
पावली के बाद से वायु प्रदूषण की मार झेल रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के खेकड़ा, बुराडी, उत्तरी करोल बाग, मयूर विहार आदि क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से 28 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की गई। हालांकि प्रयास असफल रहा। क्या है यह ‘क्लाउड सीडिंग’ ? यह ये कैसे होता है ? और क्या पर्यावरण पर इसका कुछ नकारात्मक असर भी हो सकता है?
1. क्या है क्लाउड सीडिंग और यह पहली बार कब की गई ?
क्लाउड सीडिंग एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें बादलों को बरसने के लिए प्रेरित किया जाता है। सामान्य रूप से बादल तब बारिश लाते हैं, जब उनमें नमी इतनी अधिक हो जाती है कि जलकण आपस में मिलकर भारी बूंदों में बदल जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरते हैं। लेकिन कई बार वातावरण में पर्याप्त नमी और बादल मौजूद होने के बावजूद बारिश नहीं होती। ऐसे में क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, ताकि कृत्रिम रूप से वर्षा की संभावना बढ़ाई जा सके।
सबसे पहले 1946 में अमेरिका के वैज्ञानिक विन्सेंट शेफर और इविंग लैंगम्यूर ने इस तकनीक का सफल प्रयोग किया था। उन्होंने ड्राई आइस का उपयोग कर बादलों में बर्फीले क्रिस्टल बनाए और पहली बार कृत्रिम बारिश कराई। बाद में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इस तकनीक को व्यावहारिक रूप देने का काम शुरू किया। तब से यह तकनीक धीरे-धीरे दुनिया के कई देशों में अपनाई जाने लगी। भारत में इस विषय पर शुरुआती प्रयोग 80 के दशक में किए गए, लेकिन 2000 के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित राज्यों में इसका अधिक व्यावहारिक उपयोग शुरू हुआ।
2. क्लाउड सीडिंग से बारिश आखिर कैसे होती है?
क्लाउड सीडिंग में वैज्ञानिक विशेष रासायनिक पदार्थ बादलों में छोड़ते हैं ताकि वे ‘कंडेंसेशन न्यूक्लियस’ यानी संघनन के केंद्र बन सकें। जब जलवाष्प इन कणों पर संघनित होती है तो जलकणों का आकार बढ़ने लगता है और अंततः बूंदों में बदलकर नीचे गिरते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतः तीन रसायनों सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस अथवा कार्बन डाईऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इनमें सिल्वर आयोडाइड बर्फ के क्रिस्टल जैसे ढांचे बनाता है, जिससे ठंडे बादलों में बर्फ के बीज तैयार होते हैं। वहीं सोडियम क्लोराइड गर्म बादलों में जलवाष्प को आकर्षित कर बूंदों के संघनन को बढ़ाता है, जबकि ड्राई आइस बादलों के तापमान को तेजी से घटाकर उनमें ठोस कणों का निर्माण करती है। वैज्ञानिक इन रसायनों को एयरक्राफ्ट, ड्रोन या रॉकेट के माध्यम से बादलों के भीतर छोड़ते हैं। ये कण वहां सूक्ष्म बर्फ या जलकणों को आपस में जोड़कर उनका आकार बढ़ाते हैं। जब कण पर्याप्त भारी हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वे वर्षा की बूंदों में बदल जाते हैं। यह ध्यान देना जरूरी है कि क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त बादल पहले से मौजूद होना जरूरी है। यह तकनीक ‘सूखी हवा’ से बारिश पैदा नहीं कर सकती।
3. दोनों बारिश में क्या अंतर होता है?
दोनों बारिश का मूल सिद्धांत समान है। दोनों में जलवाष्प का संघनन और बूंदों का बनना शामिल है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्राकृतिक बारिश में ये प्रक्रियाएं स्वतः होती हैं, जबकि क्लाउड सीडिंग में इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रेरित किया जाता है। सामान्य बारिश तब होती है, जब बादलों में नमी संतृप्त स्तर तक पहुंच जाती है और तापमान में गिरावट से संघनन शुरू हो जाता है। लेकिन जब यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती तो वैज्ञानिक क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बीज डालकर उसे तेज कर देते हैं।
4. सामान्य बारिश से इसका पानी भिन्न होता है?
वैज्ञानिकों के अनुसार, क्लाउड सीडिंग से हुई बारिश का पानी रासायनिक रूप से लगभग वैसा ही होता है जैसा सामान्य वर्षा का पानी। अंतर सिर्फ यह है कि इसमें रासायनिक बीज (जैसे सिल्वर आयोडाइड) के अंश बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जा सकते हैं।अधिकांश अध्ययनों में यह मात्रा एक माइक्रोग्राम प्रति लीटर से भी कम पाई गई है, जो पर्यावरण या स्वास्थ्य के
लिए हानिकारक नहीं मानी जाती।
5. पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है?
लगभग 50 से अधिक देश क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। अमेरिका इसे बर्फबारी बढ़ाने और जलाशयों को भरने के लिए करता है। चीन ने 2008 में बीजिंग ओलिम्पिक के दौरान इसका उपयोग बारिश रोकने के लिए किया था। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इसे रेगिस्तानी इलाकों में जल संकट कम करने के लिए नियमित रूप से करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे सूखा राहत कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया गया है। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ने पिछले कुछ वर्षोंसमें इस तकनीक का प्रयोग किया है। विशेष रूप से पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने 2017-2018 में व्यापक ट्रायल किए और पाया कि क्लाउड सीडिंग से वर्षा की संभावना लगभग 10-20% तक बढ़ाई जा सकती है। इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर मतभेद हैं।सकुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इससे स्थानीय मौसम चक्र प्रभावित हो सकते हैं या कुछ क्षेत्रों में वर्ष असंतुलित हो सकती है। 2021 में अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक समीक्षा रिपोर्ट ने कहा कि सीडिंग को जलवायु समाधान नहीं माना जा सकता, यह केवल अस्थायी राहत देने वाली तकनीक है।
———————–
बादल यानि मेघ, आसमान की खूबसूरती में चार चाँद लगा देते है. कई बार तो बादलों में अजीब तरह की आकृति भी नजर आने लगती है. आप जानेंगे बादल क्या है, बादल कैसे बनते हैं, बादल के प्रकार, बादल फटना से लेकर चलने, उड़ने तक सब जानकारी और रोचक तथ्य –
बादल क्या है, बादल कैसे बनते हैं, बादल के प्रकार..
1. बादल बनने में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक लग सकते है. ये लंबे और चौड़े किसी भी आकार के हो सकते है।
2. बादल मुख्यतः 3 तरह के होते है: Cumulus cloud (3300 ft. तक), Stratus cloud (6000 ft. तक) और Cirrus cloud (16500 ft. तक) होते है।
3. धुंध भी एक तरह का बादल ही है और यह जमीन के बहुत करीब होता है. धुंध में चलना.. बादलों में चलने जैसा ही है।
4. बादल पानी की छोटी-छोटी बूंदो और बर्फ के क्रिस्टल से मिलकर बना होता है. बादल में जो पानी होता है वह समुद्रो, नदियों, तालाबों और झीलों से आता है. यह पानी सूर्य की किरणों से गर्म होकर ऊपर उठता है, ऊपर आकाश में हवा ठंडी होती है वहाँ ये पानी की छोटी-छोटी बूंद बन जाता है. ये पानी की बूँद हवा में मौजूद धूल के छोटे-छोटे कण से चिपक जाती है और ऐसे ही अरबों बूँद चिपककर एक बादल का निर्माण करती है. जब इन बूंदो का वज़न ज्यादा हो छाता है तब ये आसमान से गिरने लगती है।
5. ऐसा नही है कि बादलों में वजन नही होता, एक बादल का वजन लगभग 5 लाख किलो यानि एक हवाई जहाज़ या 100 हाथियों के बराबर होता है. यह 1-1.5 किलोमीटर लंबा-चौड़ा हो सकता है.
6. बादल सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते है इसलिए सफेद दिखाई देते है।
7. बादल 146 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ सकते है यानि एक बादल को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 9 घंटे लगेगे।
8. जिस भी ग्रह पर वातावरण है वहाँ बादल है.. लेकिन पानी के नही. शुक्र ग्रह पर sulphur oxide और आपको जानकर हैरानी होगी कि शनि और बृहस्पति ग्रह पर अमोनियों के बादल है.
9. फ्लाइट का लेट या रद्द होना ‘Cumulonimbus’ बादलों की वजह से होता है. यह बिजली कड़काने से लेकर.. तूफान, ओले और कभी-कभी बवंडर भी लाने में सक्षम है।
10. नक्षत्रमंडल बादल (Noctilucent Clouds ) 75 से 85 km की ऊँचाई पर होते है. ये इतने ऊँचे है कि रात को भी सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं।
11. ईरान में बादलों को भाग्यशाली माना जाता है. यहाँ किसी को आशीर्वाद देते समय ‘Your sky is always filled with clouds’ कहा जाता है।
12.दुनिया में सबसे ज्यादा बादलों से घिरा हुआ स्थान अंटार्कटिक हिंद महासागर का साउथ अफ्रिकाप्रिंस आइसलैंड है. यहाँ साल के 8760 घंटो में से सिर्फ 800 घंटे धूप निकलती है।
बादल फटना
13. जिस जगह पर 100mm यानि 4 इंच से ज्यादा बारिश हो जाए उसे बादल फटना कहते है.. बादल फटने के कारण सबसे अधिक बाढ़ 8 January 1966 को गंगा डेल्टा में आई थी. इसका कुछ भाग भारत और कुछ बांग्लादेश में है. यहाँ 2329mm बारिश हुई थी. 1 July, 2016 को उतराखंड में बादल फटने से 1372mm बारिश हुई थी. जब गर्म हवा के कारण बूंदे नीचे की बजाय ऊपर उठने लगती है और जब ये बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर बादल फटने की ज्यादा संभावना रहती है. अधिकतर बादल जमीन से 14000 फीट की ऊंचाई पर और पहाड़ो से टकराने की वजह से फटते है।
बादल स्लेटी रंग के क्यों होते है ?
14. जब अरबों पानी की बूंदो के साथ बादल बहुत मोटे हो जाते है तब सूर्य की रोशनी इनमें चमक नही हो पाती और ये स्लेटी नज़र आने लगते है. बादलों के स्लेटी होते ही हमें समझ जाना चाहिए कि बारिश होने वाली है।
गुरूत्वाकर्षण बल के कारण बादल नीचे क्यों नही गिरते ?
15. बादल बहुत छोटी-छोटी यानि 1 माइक्रोन साइज़ जितनी बूंदो से मिलकर बना होता है. बूँद इतनी हल्की होने के कारण gravity को सही से रिस्पोंड नही करती और यही बात पूरे बादल पर भी लागू होती है।
आकाश में बादल चलते है या फिर पृथ्वी घूम रही है ?
16. बादल चलते है और इनके चलने का कारण हवा है. धरती हमेशा एक ही दिशा में घूमती है लेकिन बादल नही. अगर बादल नही चलते तो ये भी पृथ्वी की तरह एक ही दिशा में घूमते. लेकिन हाँ, पृथ्वी का घूमना बादलों के चलने को थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर करता है।
■■■■
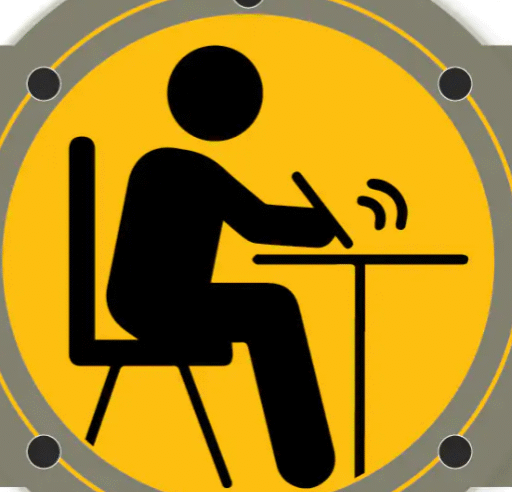
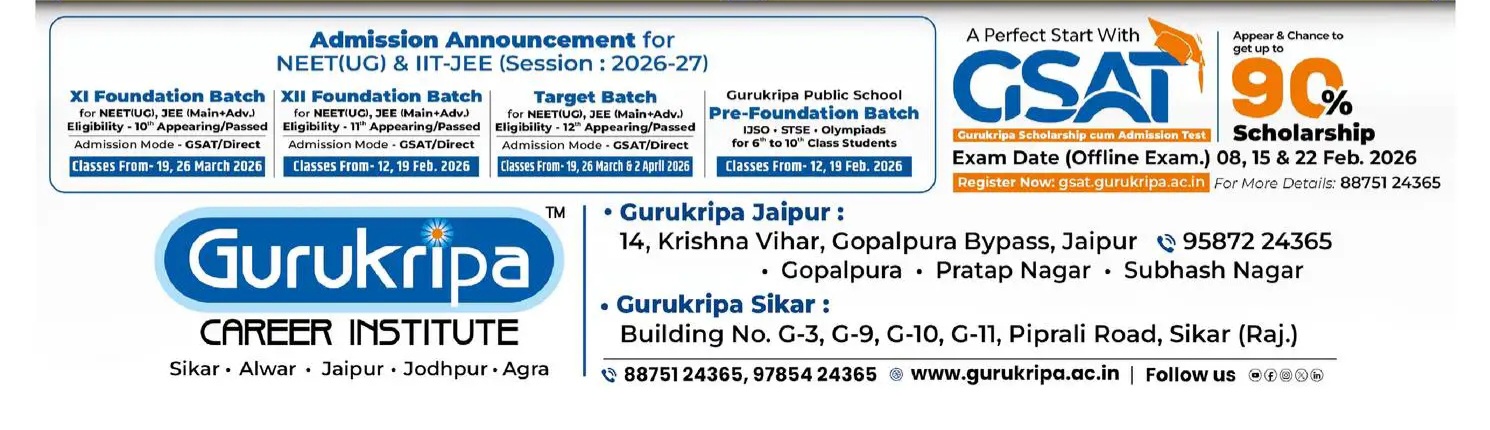
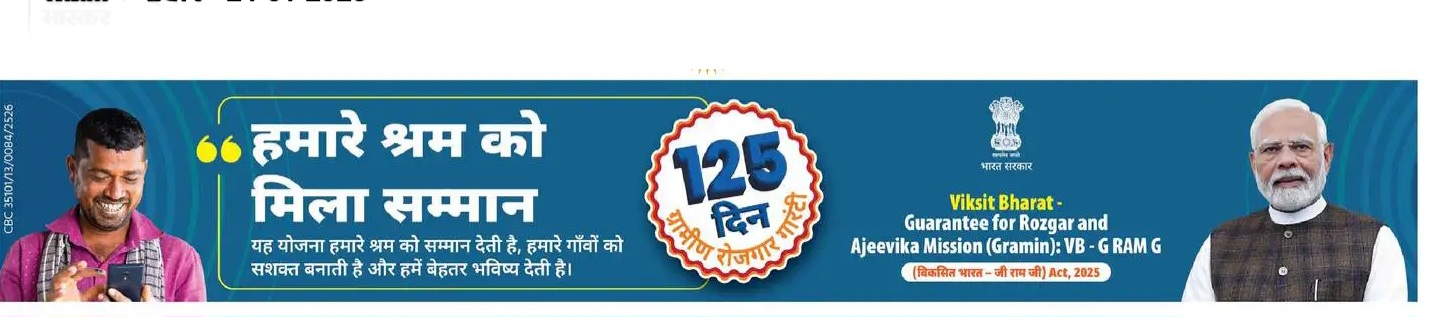

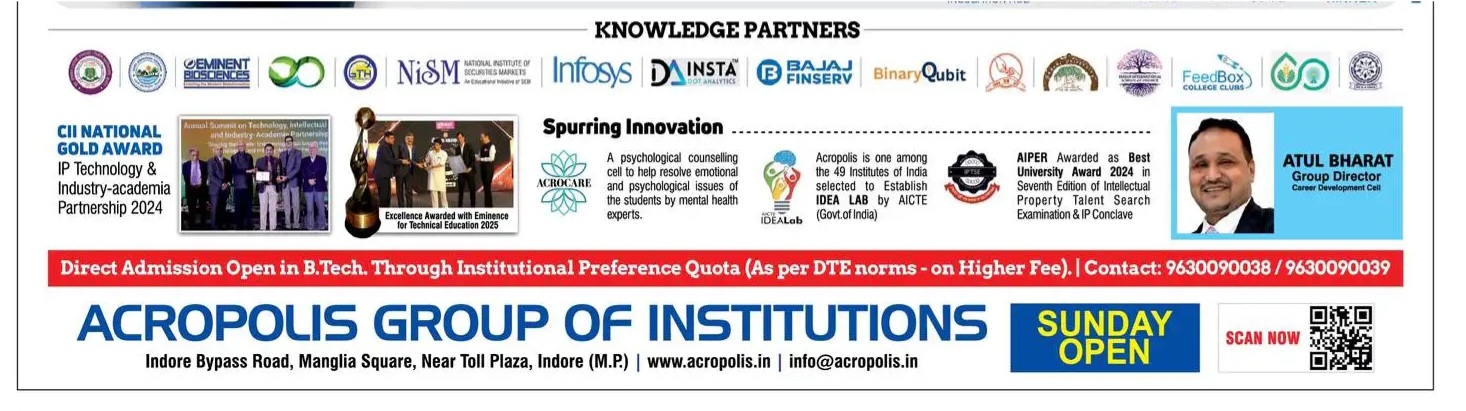




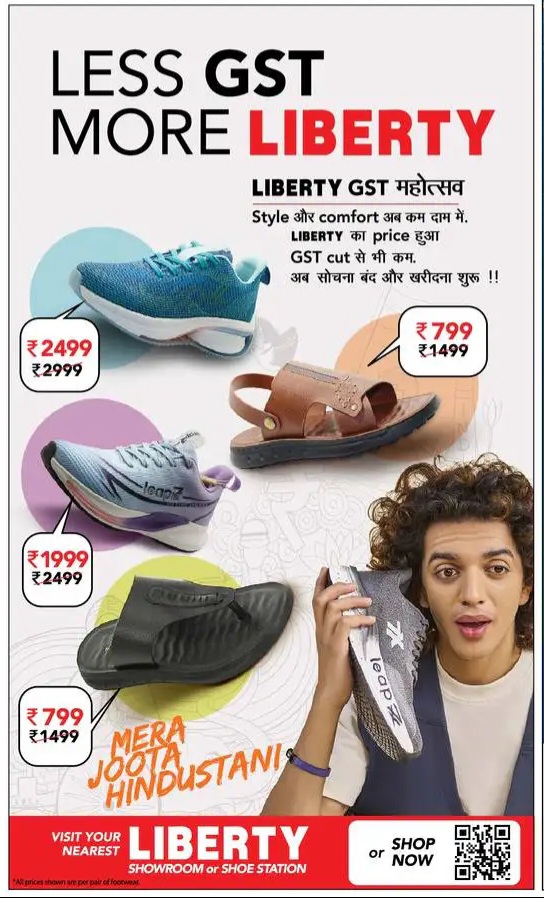

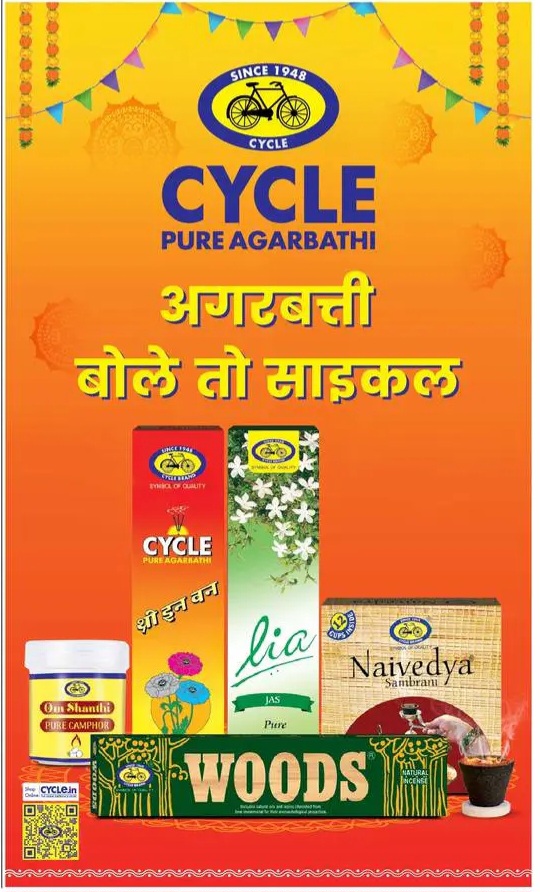
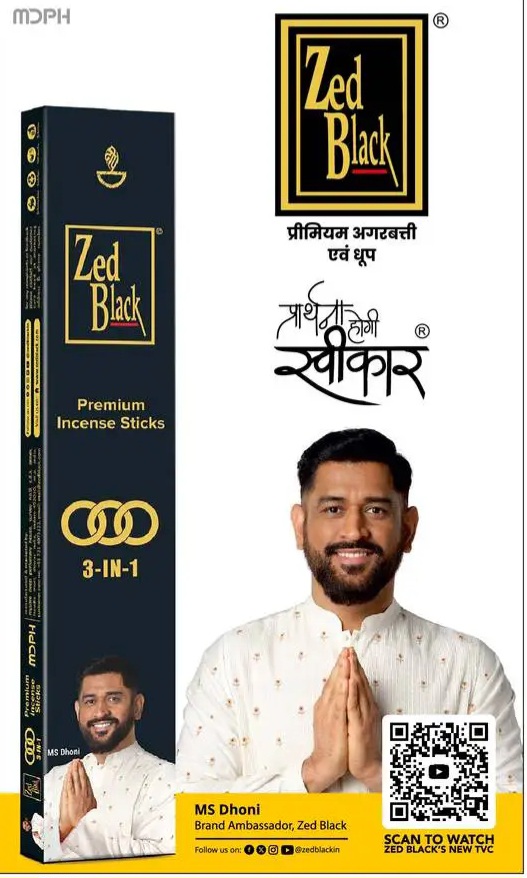
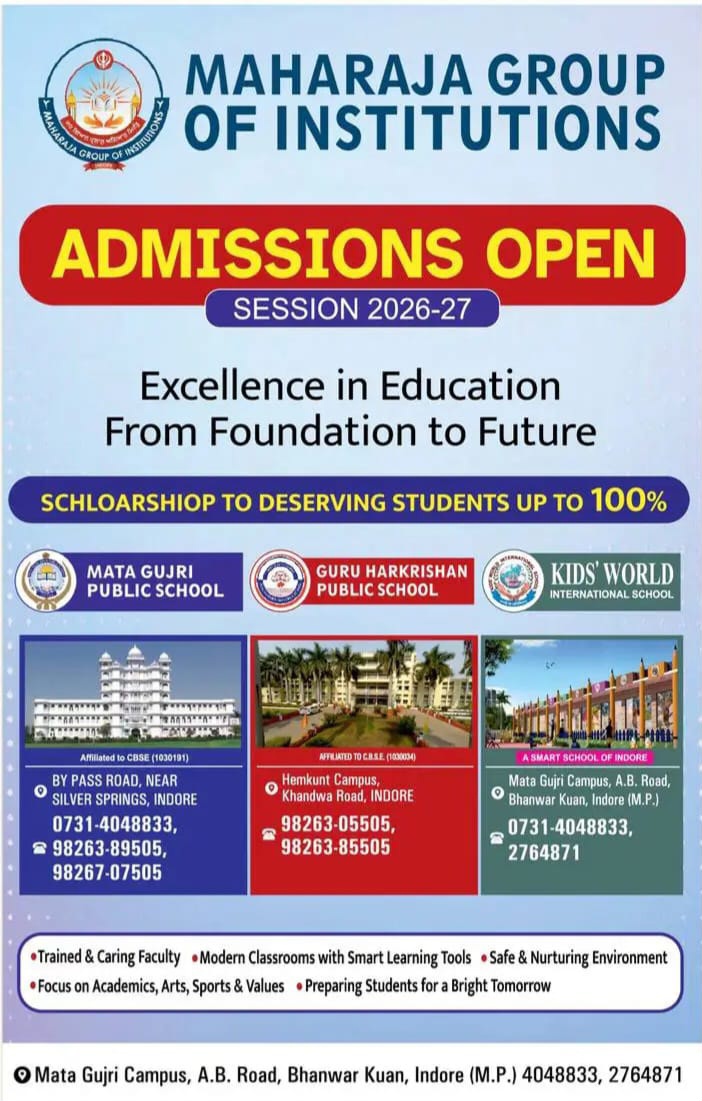
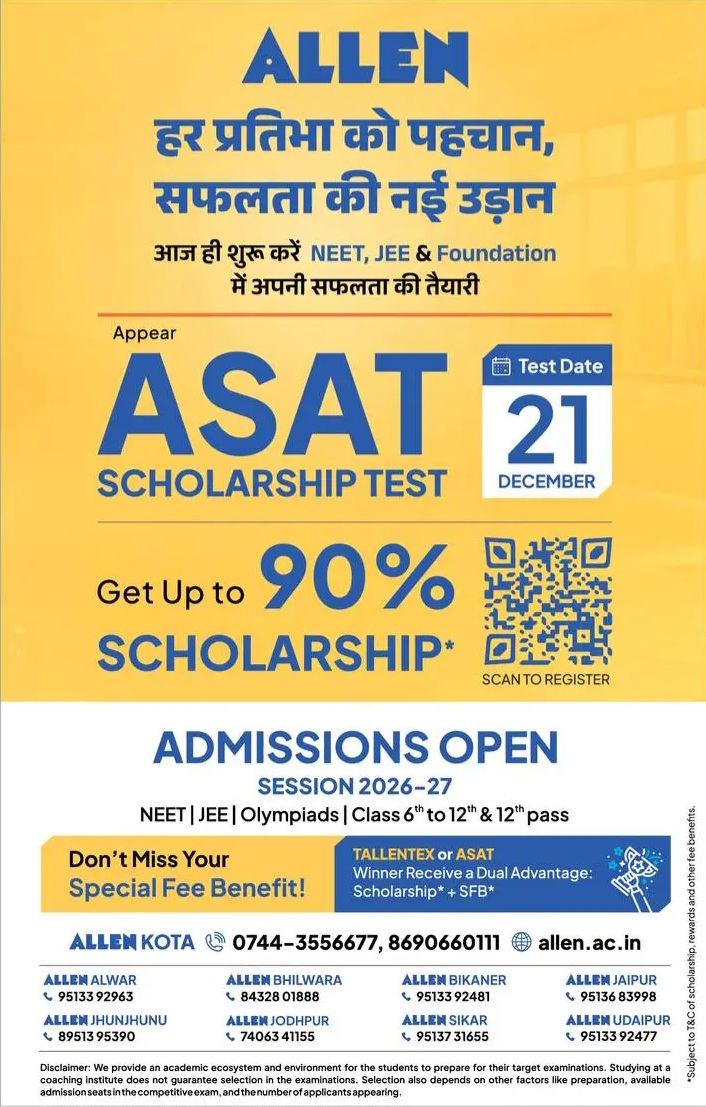
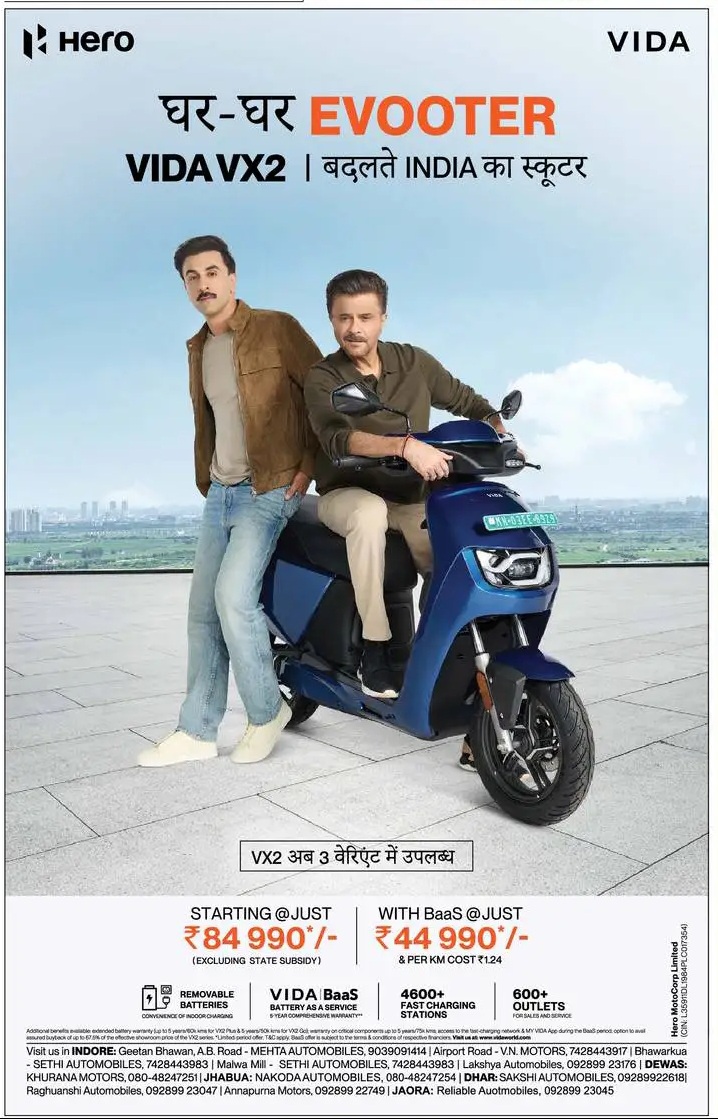
 +91-94068 22273
+91-94068 22273 
